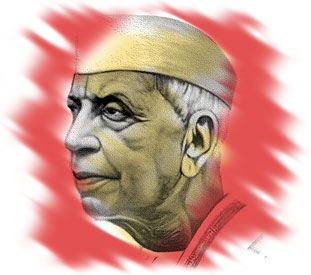प्रथम सर्ग
– (१) –
अयि दयामयि देवि, सुखदे, सारदे,
इधर भी निज वरद-पाणि पसारदे।
दास की यह देह-तंत्री तार दे,
रोम-तारों में नई झंकार दे।
बैठ मानस-हंस पर कि सनाथ हो,
भार-वाही कंठ-केकी साथ हो।
चल अयोध्या के लिए सज साज तू,
मां, मुझे कृतकृत्य कर दे आज तू।
स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया,
भाग्यभास्कर उदयगिरि पर चढ़ गया।
हो गया निर्गुण सगुण-साकार है;
ले लिया अखिलेश ने अवतार है।
किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया?
मनुज बनकर मानवी का पय पिया?
भक्त-वत्सलता इसीका नाम है।
और वह लोकेश लीला-धाम है।
पथ दिखाने के लिए संसार को,
दूर करने के लिए भू-भार को,
सफल करने के लिए जन-दृष्टियाँ,
क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियाँ?
असुर-शासन शिशिर-मय हेमंत है;
पर निकट ही राम-राज्य-वसंत है।
पापियों का जान लो अब अंत है,
भूमि पर प्रकटा अनादि-अनंत है।
राम-सीता, धन्य धीरांबर-इला,
शौर्य-सह संपत्ति, लक्ष्मण-उर्मिला।
भरत कर्त्ता, मांडवी उनकी क्रिया;
कीर्ति-सी श्रुतकीर्ति शत्रुघ्नप्रिया।
ब्रह्म की हैं चार जैसी स्फूर्तियाँ,
ठीक वैसी चार माया-मूर्त्तियाँ,
धन्य दशरथ-जनक-पुण्योत्कर्ष है;
धन्य भगवद्भूमि-भारतवर्ष है!
देख लो, साकेत नगरी है यही,
स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही।
केतु-पट अंचल-सदृश हैं उड़ रहे,
कनक-कलशों पर अमर-दृग जुड़ रहे।
सोहती हैं विविध-शालाएँ बड़ी;
छत उठाए भित्तियाँ चित्रित खड़ी।
गेहियों के चारु-चरितों की लड़ी,
छोड़ती है छाप, जो उन पर पड़ी!
स्वच्छ, सुंदर और विस्तृत घर बनें,
इंद्रधनुषाकार तोरण हैं तनें।
देव-दंपति अट्ट देख सराहते;
उतर कर विश्राम करना चाहते।
फूल-फल कर, फैल कर जो हैं बढ़ी,
दीर्घ छज्जों पर विविध बेलें चढ़ीं।
पौरकन्याएँ प्रसून-स्तूप कर,
वृष्टि करती हैं यहीं से भूप पर।
फूल-पत्ते हैं गवाक्षों में कढ़े,
प्रकृति से ही वे गए मानो गढ़े।
दामनी भीतर दमकती है कभी,
चंद्र की माला चमकती है कभी।
सर्वदा स्वच्छंद छज्जों के तले,
प्रेम के आदर्श पारावत पले।
केश-रचना के सहायक हैं शिखी,
चित्र में मानों अयोध्या है लिखी!
दृष्टि में वैभव भरा रहता सदा;
घ्राण में आमोद है बहता सदा।
ढालते हैं शब्द श्रुतियों में सुधा;
स्वाद गिन पाती नहीं रसना-क्षुधा!
कामरूपी वारिदों के चित्र-से,
इंद्र की अमरावती के मित्र-से,
कर रहे नृप-सौध गगम-स्पर्श हैं;
शिल्प-कौशल के परम आदर्श हैं।
कोट-कलशों पर प्रणीत विहंग हैं;
ठीक जैसे रूप, वैसे रंग हैं।
वायु की गति गान देती है उन्हें;
बाँसुरी की तान देती है उन्हें।
ठौर ठौर अनेक अध्वर-यूप हैं,
जो सुसंवत् के निदर्शन-रूप हैं।
राघवों की इंद्र-मैत्री के बड़े,
वेदियों के साथ साक्षी-से खड़े।
मूर्तिमय, विवरण समेत, जुदे जुदे,
ऐतिहासिक वृत्त जिनमें हैं खुदे,
यत्र तत्र विशाल कीर्ति-स्तंभ हैं,
दूर करते दानवों का दंभ हैं।
– (२) –
स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ
किंतु सुरसरिता कहाँ, सरयू कहाँ?
वह मरों को मात्र पार उतारती;
यह यहीं से जीवितों को तारती!
अंगराग पुरांगनाओं के धुले,
रंग देकर नीर में जो हैं घुले,
दीखते उनसे विचित्र तरंग हैं;
कोटि शक्र-शरास होते भंग हैं।
है बनी साकेत नगरी नागरी,
और सात्विक-भाव से सरयू भरी।
पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही;
कर्ण-कोमल कल-कथा-सी कह रही।
तीर पर हैं देव-मंदिर सोहते;
भावुकों के भाव मन को मोहते।
आस-पास लगी वहाँ फुलवारियाँ;
हँस रही हैं खिलखिला कर क्यारियाँ।
है अयोध्या अवनि की अमरावती,
इंद्र हैं दशरथ विदित वीरव्रती,
वैजयंत विशाल उनके धाम हैं,
और नंदन वन बने आराम हैं।
एक तरु के विविध सुमनों-से खिले,
पौरजन रहते परस्पर हैं मिले।
स्वस्थ, शिक्षित, शिष्ट उद्योगी सभी,
बाह्यभोगी, आंतरिकयोगी सभी।
व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए;
आधि की शंका नहीं मन के लिए।
चोर की चिंता नहीं धन के लिए;
सर्व सुख हैं प्राप्त जीवन के लिए।
एक भी आँगन नहीं ऐसा यहाँ,
शिशु न करते हों कलित-क्रीडा जहाँ।
कौन है ऐसा अभागा गृह कहो,
साथ जिसके अश्व-गोशाला न हो?
धान्य-धन-परिपूर्ण सबके धाम हैं,
रंगशाला-से सजे अभिराम हैं।
नागरों की पात्रता, नव नव कला,
क्यों न दे आनंद लोकोत्तर भला?
ठाठ है सर्वत्र घर या घाट है;
लोक-लक्ष्मी की विलक्षण हाट है।
सिक्त, सिंजित-पूर्ण मार्ग अकाट्य हैं;
घर सुघर नेपथ्य, बाहर नाट्य है!
अलग रहती हैं सदा ही ईतियाँ;
भटकती हैं शून्य में ही भीतियाँ।
नीतियों के साथ रहती रीतियाँ;
पूर्ण हैं राजा-प्रजा की प्रीतियाँ।
पुत्र रूपी चार फल पाए यहीं;
भूप को अब और कुछ पाना नहीं।
बस यही संकल्प पूरा एक हो,
शीघ्र ही श्रीराम का अभिषेक हो।
सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ;
किंतु समझो, रात का जाना हुआ।
क्योंकि उसके अंग पीले पड़ चले;
रम्य-रत्नाभरण ढीले पड़ चले।
एक राज्य न हो, बहुत से हों जहाँ,
राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ।
बहुत तारे थे, अँधेरा कब मिटा,
सूर्य का आना सुना जब, तब मिटा।
नींद के भी पैर हैं कँपने लगे;
देखलो, लोचन-कुमुद झँपने लगे।
वेष-भूषा साज ऊषा आ गई;
मुख-कमल पर मुस्कराहट छा गई।
पक्षियों की चहचहाहट हो उठी,
चेतना की अधिक आहट हो उठी,
स्वप्न के जो रंग थे वे घुल उठे,
प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे।
दीप-कुल की ज्योति निष्प्रभ हो निरी,
रह गई अब एक घेरे में घिरी।
किंतु दिनकर आ रहा, क्या सोच है?
उचित ही गुरुजन-निकट संकोच है।
हिम-कणों ने है जिसे शीतल किया,
और सौरभ ने जिसे नव बल दिया,
प्रेम से पागल पवन चलने लगा;
सुमन-रज सर्वांग में मलने लगा!
प्यार से अंचल पसार हरा-भरा,
तारकाएँ खींच लाई है धरा।
निरख रत्न हरे गए निज कोष के,
शून्य रंग दिखा रहा है रोष के।
ठौर ठौर प्रभातियाँ होने लगीं,
अलसता की ग्लानियाँ धोने लगीं।
कौन भैरव-राग कहता है इसे,
श्रुति-पुटों से प्राण पीते हैं जिसे?
दीखते थे रंग जो धूमिल अभी,
हो गए हैं अब यथायथ वे सभी।
सूर्य के रथ में अरुण-हय जुत गए,
लोक के घर-वार ज्यों लिप-पुत गए।
सजग जन-जीवन उठा विश्रांत हो,
मरण जिसको देख जड़-सा भ्रांत हो।
दधिविलोडन, शास्त्रमंथन सब कहीं;
पुलक-पूरित तृप्त तन-मन सब कहीं।
खुल गया प्राची दिशा का द्वार है,
गगन-सागर में उठा क्या ज्वार है!
पूर्व के ही भाग्य का यह भाग है,
या नियति का राग-पूर्ण सुहाग है!
अरुण-पट पहने हुए आह्लाद में,
कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में?
प्रकट-मूर्तिमती उषा ही तो नहीं?
कांति-की किरणें उजेला कर रहीं।
यह सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नई,
आप विधि के हाथ से ढाली गई।
कनक-लतिका भी कमल-सी कोमला,
धन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला!
जान पड़ता नेत्र देख बड़े-बड़े-
हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े।
– (३ ) –
पद्मरागों से अधर मानों बने;
मोतियों से दाँत निर्मित हैं घने।
और इसका हृदय किससे है बना?
वह हृदय ही है कि जिससे है बना।
प्रेम-पूरित सरल कोमल चित्त से,
तुल्यता की जा सके किस वित्त से?
शाण पर सब अंग मानो चढ़ चुके,
प्राण फिर उनमें पड़े जब गढ़ चुके।
झलकता आता अभी तारुण्य है,
आ गुराई से मिला आरुण्य है!
लोल कुंडल मंडलाकृति गोल हैं,
घन-पटल-से केश, कांत-कपोल हैं।
देखती है जब जिधर यह सुंदरी,
दमकती है दामिनी-सी द्युति-भरी।
हैं करों में भूरि भूरि भलाइयाँ,
लचक जाती अन्यथा न कलाइयाँ?
चूड़ियों के अर्थ, जो हैं मणिमयी,
अंग की ही कांति कुंदन बन गई।
एक ओर विशाल दर्पण है लगा,
पार्श्व से प्रतिबिंब जिसमें है जगा।
मंदिरस्था कौन यह देवी भला?
किस कृती के अर्थ है इसकी कला?
स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला;
नाम है इसका उचित ही “उर्मिला”।
शील-सौरभ की तरंगें आ रही,
दिव्य-भाव भवाब्धि में हैं ला रही।
सौधसिंहद्वार पर अब भी वही,
बाँसुरी रस-रागिनी में बज रही।
अनुकरण करता उसी का कीर है,
पंजरस्थित जो सुरम्य शरीर है।
उर्मिला ने कीर-सम्मुख दृष्टि की,
या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि की!
मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ,
रह गया वह देखता-सा स्थित हुआ!
प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा–
“रे सुभाषी, बोल, चुप क्यों हो रहा?”
पार्श्व से सौमित्रि आ पहुँचे तभी,
और बोले-“लो, बता दूँ मैं अभी।
नाक का मोती अधर की कांति से,
बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से,
देख कर सहसा हुआ शुक मौन है;
सोचता है, अन्य शुक यह कौन है?”
यों वचन कहकर सहास्य विनोद से,
मुग्ध हो सौमित्रि मन के मोद से,
पद्मिनी के पास मत्त-मराल-से,
होगए आकर खड़े स्थिर चाल से।
चारु-चित्रित भित्तियाँ भी वे बड़ी,
देखती ही रह गईं मानों खड़ी।
प्रीति से आवेग मानों आ मिला,
और हार्दिक हास आँखों में खिला।
मुस्करा कर अमृत बरसाती हुई,
रसिकता में सुरस सरसाती हुई,
उर्मिला बोली, “अजी, तुम जग गए?
स्वप्न-निधि से नयन कब से लग गए?”
“मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ,
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ!”
गत हुई संलाप में बहु रात थी,
प्रथम उठने की परस्पर बात थी।
“जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं!”
“प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं!”
– (४) –
“प्रेम की यह रुचि विचित्र सराहिए,
योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए?”
“धन्य है प्यारी, तुम्हारी योग्यता,
मोहिनी-सी मूर्त्ति, मंजु-मनोज्ञता।
धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ;
किन्तु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ।”
“दास बनने का बहाना किस लिए?
क्या मुझे दासी कहाना, इस लिए?
देव होकर तुम सदा मेरे रहो,
और देवी ही मुझे रक्खो, अहो!”
उर्मिला यह कह तनिक चुप हो रही;
तब कहा सौमित्रि ने कि “यही सही।
तुम रहो मेरी हृदय-देवी सदा;
मैं तुम्हारा हूँ प्रणय-सेवी सदा।”
फिर कहा–“वरदान भी दोगी मुझे?
मानिनी, कुछ मान भी दोगी मुझे?”
उर्मिला बोली कि “यह क्या धर्म है?
कामना को छोड़ कर ही कर्म है!”
“किन्तु मेरी कामना छोटी-बड़ी,
है तुम्हारे पाद-पद्मों में पड़ी।
त्याग या स्वीकार कुछ भी हो भले,
वह तुम्हारी वस्तु आश्रित-वत्सले!”
“शस्त्रधारी हो न तुम, विष के बुझे,
क्यों न काँटों में घसीटोगे मुझे!
अवश अबला हूँ न मैं, कुछ भी करो,
किन्तु पैर नहीं, शिरोरुह तब धरो!”
“साँप पकड़ाओ न मुझको निर्दये,
देख कर ही विष चढ़े जिनका अये!
अमृत भी पल्लव-पुटों में है भरा,
विरस मन को भी बना दे जो हरा।
’अवश-अबला’ तुम? सकल बल-वीरता,
विश्व की गम्भीरता, घ्रुव-धीरता,
बलि तुम्हारी एक बाँकी दृष्टि पर,
मर रही है, जी रही है सृष्टि भर!
भूमि के कोटर, गुहा, गिरि, गर्त्त भी,
शून्यता नभ की, सलिल-आवर्त्त भी,
प्रेयसी, किसके सहज-संसर्ग से,
दीखते हैं प्राणियों को स्वर्ग-से?
जन्म-भूमि-ममत्व कृपया छोड़ कर,
चारु-चिन्तामणि-कला से होड़ कर,
कल्पवल्ली-सी तुम्हीं चलती हुई,
बाँटती हो दिव्य-फल फलती हुई!”
“खोजती हैं किन्तु आश्रय मात्र हम,
चाहती हैं एक तुम-सा पात्र हम,
आन्तरिक सुख-दुःख हम जिसमें धरें,
और निज भव-भार यों हलका करें।
तदपि तुम–यह कीर क्या कहने चला?
कह अरे, क्या चाहिए तुझको भला?”
“जनकपुर की राज-कुंज-विहारिका,
एक सुकुमारी सलौनी सारिका!”
देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण हँसे;
उर्मिला के नेत्र खंजन-से फँसे।
“तोड़ना होगा धनुष उसके लिए”;
“तोड़ डाला है उसे प्रभु ने प्रिये!
सुतनु, टूटे का भला क्या तोड़ना?
कीर का है काम दाडिम फोड़ना,–
होड़ दाँतों की तुम्हारे जो करे,
जन्म मिथिला या अयोध्या में धरे!”
ललित ग्रीवा-भंग दिखला कर अहा!
उर्मिला ने लक्ष कर प्रिय को, कहा–
“और भी तुमने किया है कुछ कभी,
या कि सुग्गे ही पढ़ाये हैं अभी?”
“बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही!”
बात यह सौमित्रि ने सस्मित कही।
“देख लूँगी” उर्मिला ने भी कहा।
विविध विध फिर भी विनोदामृत बहा।
हार जाते पति कभी, पत्नी कभी;
किन्तु वे होते अधिक हर्षित तभी।
प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है,
हार में जिसमें परस्पर जीत है!
“कल प्रिये, निज आर्य का अभिषेक है;
सब कहीं आनन्द का अतिरेक है।
राम-राज्य विधान होने जा रहा;
पूत पर पावन नया युग आ रहा!
अब नया वर-वेश होगा आर्य का,
और साधन क्षत्र-कुल के कार्य का।
दृग सफल होंगे हमारे शीघ्र ही,
सिद्ध होंगे सुकृत सारे शीघ्र ही।”
“ठीक है, पर कुछ मुझे देना कहो,
सेंत मेंत न दृष्टि-फल लेना कहो,
तो तुम्हें अभिषेक दिखला दूँ अभी,
दृश्य उसका सामने ला दूँ अभी।”
“चित्र क्या तुमने बनाया है अहा?”
हर्ष से सौमित्रि ने साग्रह कहा–
“तो उसे लाओ, दिखाओ, है कहाँ?
’कुछ’ नहीं मैं ’बहुत कुछ’ दूँगा यहाँ।”
उर्मिला ने मूर्ति बन कर प्रेम की,
खींच कर मणि-खचित मचिया हेम की,
आप प्रियतम को बिठा उस पर दिया,
और ला कर चित्रपट सम्मुख किया।
चित्र भी था चित्र और विचित्र भी,
रह गये चित्रस्थ-से सौमित्र भी।
– (५) –
देख भाव-प्रवणता, वर-वर्णता,
वाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता!
तूलिका सर्वत्र मानों थी तुली;
वर्ण-निधि-सी व्योम-पट पर थी खुली।
चित्र के मिष, नेत्र-विहगों के लिए,
आप मोहन-जाल माया थी लिये।
सुध न अपनी भी रही सौमित्र को;
देर तक देखा किये वे चित्र को।
अन्त में बोले बड़े ही प्रेम से–
“हे प्रिये, जीती रहो तुम क्षेम से।
दुर्ग-सम्मुख, दृष्टि-रोध न हो जहाँ,
है सभा-मण्डप बना विस्तृत वहाँ।
झालरों में मंजु मुक्ता हैं पुहे,
माँग में जिस भाँति जाते हैं गुहे।
दीर्घ खम्भे हैं बने वैदूर्य के;
ध्वज-पटों में चिन्ह कुल-गुरु सूर्य के।
बज रही है द्वार पर जय-दुन्दभी,
और प्रहरी हैं खड़े प्रमुदित सभी।
क्षौम के छत में लटकते गुच्छ हैं,
सामने जिनके चमर भी तुच्छ हैं।
पद्म-पुंजों-से पटासन हैं पड़े,
और हैं बाघंबरों के पाँवड़े।
बीच में है रत्न-सिंहासन बना,
छन्न और वितान जिस पर है तना।
आर्यदम्पति राजते अभिराम हैं,
प्रकट तुलसी और शालिग्राम हैं!
सब सभासद शिष्ट हैं, नय-निष्ठ हैं;
छोड़ते अभिषेक-वारि वसिष्ठ हैं।
आर्य-आर्या हैं तनिक कैसे झुके,
आज मानों लोक-भार उठा चुके!
बरसती है खचित मणियों की प्रभा;
तेज में डूबी हुई है सब सभा!
सुर-सभा-गृह बिम्ब इसका ही बड़ा,
व्योम-रूपी काच में है जा पड़ा!
पंच-पुरजन-सचिव सब प्रमुदित बड़े;
माण्डलिक नरवीर कैसे हैं खड़े।
हाथ में राजोपहार लिये हुए,
देश-देश-विचित्र-वेश किये हुए।
किन्तु मित्र नरेश सब कब आ सके?
भरत भी न यहाँ बुलाये जा सके।
यह तुम्हारी भावना की स्फूर्ति है;
जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है!
हो रहा है जो यहाँ, सो हो रहा,
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा?
किन्तु होना चाहिए कब क्या, कहाँ,
व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ।
मानते हैं जो कला के अर्थ ही,
स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही।
वह तुम्हारे और तुम उसके लिए,
चाहिए पारस्परिकता ही प्रिये!
मंजरी-सी अंगुलियों में यह कला!
देख कर मैं क्यों न सुध भूलूँ भला?
क्यों न अब मैं मत्त-गज-सा झूम लूँ?
कर-कमल लाओ तुम्हारा चूम लूँ!”
कर बढ़ा कर, जो कमल-सा था खिला,
मुस्कराई और बोली उर्मिला–
“मत्त-गज बनकर विवेक न छोड़ना,
कर कमल कह कर न मेरा तोड़ना!”
वचन सुन सौमित्रि लज्जित हो गये,
प्रेम-सागर में निमज्जित हो गये।
पकड़ कर सहसा प्रिया का कर वही,
चूम कर फिर फिर उसे बोले यही–
“एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं;
ठीक भी है, वह तुम्हें पाती नहीं।
सजग अब इससे रहूँगा मैं सदा;
अनुपमा तुमको कहूँगा मैं सदा!
निरुपमे, पर चित्र मेरा है कहाँ?”
“प्रिय, तुम्हारा कौन-सा पद है यहाँ?”
“भावती, मैं भार लूँ किस काम का?
एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का।”
“किन्तु सीता की बहन है उर्मिला;
वाह, उलटा योग यह अच्छा मिला!
अस्तु, कुछ देना तुम्हें स्वीकार हो,
तो तुम्हारा चित्र भी तैयार हो।”
“और जो न हुआ?” गिरा प्रिय ने कही;
“तो पलट कर आप मैं दूँगी वही।”
होड़ कर यों उर्मिला उद्यत हुई,
और तत्क्षण कार्य में वह रत हुई।
ज्योति-सी सौमित्रि के सम्मुख जगी;
चित्रपट पर लेखनी चलने लगी।
– (६) –
अवयवों की गठन दिखला कर नई,
अमल जल पर कमल-से फूले कई।
साथ ही सात्विक-सुमन खिलने लगे,
लेखिका के हाथ कुछ हिलने लगे!
झलक आया स्वेद भी मकरन्द-सा,
पूर्ण भी पाटव हुआ कुछ मन्द-सा।
चिबुक-रचना में उमंग नहीं रुकी,
रंग फैला, लेखनी आगे झुकी।
एक पीत-तरंग-रेखा-सी बही,
और वह अभिषेक-घट पर जा रही!
हँस पड़े सौमित्रि भावों से भरे;
उर्मिला का वाक्य था केवल “अरे!”
“रंग घट में ही गया, देखा रहो,
तुम चिबुक धरने चलीं थीं, क्यों न हो?”
उर्मिला भी कुछ लजा कर हँस पड़ी,
वह हँसी थी मोतियों की-सी लड़ी।
“बन पड़ी है आज तो!” उसने कहा–
“क्या करूँ, बस में न मेरा मन रहा।
हार कर तुम क्या मुझे देते कहो?
मैं वही दूँ, किन्तु कुछ का कुछ न हो।”
हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये,
और बोले–“एक परिरम्भण प्रिये!”
सिमिट-सी सहसा गई प्रिय की प्रिया,
एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया।
किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया,
आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया!
बीत जाता एक युग पल-सा वहाँ,
सुन पड़ा पर हर्ष-कलकल-सा वहाँ।
द्वार पर होने लगी विरुदावली;
गूँजने सहसा लगी गगनस्थली।
सूत, मागध, वन्दिजन यश पढ़ उठे,
छन्द और प्रबन्ध नूतन गढ़ उठे।
मुरज, वीणा, वेणु आदिक बज उठे;
विज्ञ वैतालिक सुरावट सज उठे।
दम्पती चौंके, पवन-मण्डल हिला;
चंचला-सी छिटक छूटी उर्मिला।
तब कहा सौमित्रि ने–“तो अब चलूँ,
याद रखना किन्तु जो बदला न लूँ?
देखने कुल-वृद्धि-सी पाताल से,
आ गये कुलदेव भी द्रुत चाल से।
दिन निकल आया, बिदा दो अब मुझे;
फिर मिले अवकाश देखूँ कब मुझे?”
उर्मिला कहने चली कुछ, पर रुकी,
और निज अंचल पकड़ कर वह झुकी।
भक्ति-सी प्रत्यक्ष भू-लग्ना हुई,
प्रिय कि प्रभु के प्रेम में मग्ना हुई।
चूमता था भूमितल को अर्द्ध विधु-सा भाल;
बिछ रहे थे प्रेम के दृग-जाल बन कर बाल।
छत्र-सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ;
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ।
इसके आगे? बिदा विशेष;
हुए दम्पती फिर अनिमेष।
किन्तु जहाँ है मनोनियोग,
वहाँ कहाँ का विरह वियोग?